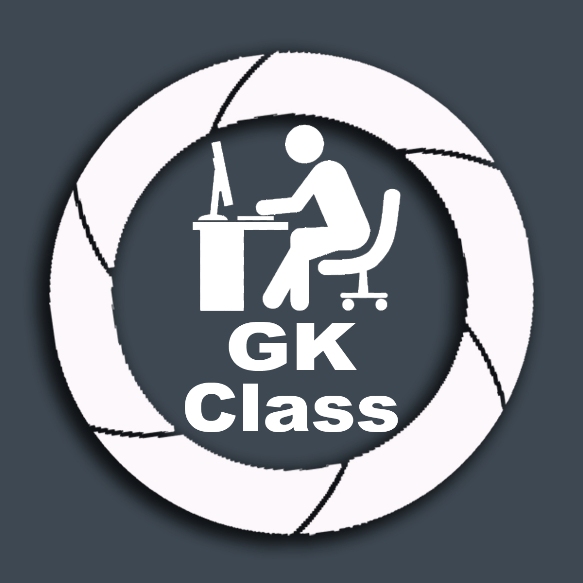भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble of The Indian Constitution)-
- भारतीय संविधान में उद्देशका या प्रस्तावना को भारत की संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को अपनाया था।
- प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है।
प्रस्तावना-
- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय तथा विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
प्रस्तावना- भारतीय संविधान का दर्शन (Preamble- Philosophy of The Indian Constitution)-
- प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है।
- प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गई है।
- 1. सम्प्रभुता (Sovereignty)
- 2. समाजवाद (Socialism)
- 3. पंथनिरपेक्षता (Secularism)
- 4. लोकतंत्र (Democracy)
- 5. गणराज्य (Republic)
- 6. न्याय (Justice)
- सम्प्रभुता से तात्पर्य है की कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो अर्थात् वह अपने सभी निर्णय स्वयम् लेता हो और किसी भी प्रकार से वह किसी अन्य देश या सत्ता के अधीन नहीं हो सम्प्रभुता कहलता है।
- 15 अगस्त, 1947 को भारत एक डोमिनियन स्टेट (Dominion State) बना। अर्थात् भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था लेकिन भारत की शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों से संचालित होती थी जैसे-
- भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान के रूप में प्रयोग किया जाता था।
- भारत में संविधान सभा ही विधायिका का कार्य भी करती थी।
- ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था।
- 26 जनवरी, 1950 को भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र बन गया था
- पाकिस्तान 1956 ई. तक डोमिनियन स्टेट बना रहा था।
- कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड अभी भी डोमिनियन स्टेट है क्योंकि ब्रिटिश क्राउन इन देशों का राष्ट्राध्यक्ष है।
- वर्तमान में लगभग सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तथा सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव को भी मानना पड़ता है। लेकिन सम्प्रभुता सीमित नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही इन्हें स्वीकार करता है। तथा यह कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को त्यागने के लिए स्वतंत्र है।
- भारत एक समाजवादी देश है परन्तु भारत का समाजवाद साम्यवाद से अलग है।
- भारत का समाजवाद हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन करता है।
- समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति को मान्यता देता है।
- समाजवाद संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है। अर्थात् योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण किया गया है।
- समाजवाद में संसाधनों के अहितकारी संकेन्द्रण का विरोध करता है।
- समाजवाद कमजोर लोगों को विशेष संरक्षण देने पर बल देता है।
- भारतीय समाजवाद फेबियन समाजवाद के नजदीक है।
साम्यवाद तथा समाजवाद में अंतर (Difference Between Communism and Socialism)-
- (I) साम्यवाद (Communism)
- (II) समाजवाद (Socialism)
- साम्यवाद हिंसक क्रांति का समर्थन करता है।
- साम्यवाद निजी सम्पत्ति का विरोध करता है।
- साम्यवाद के अनुसार संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए।
- साम्यवाद राष्ट्रवाद को नहीं मानता है।
- साम्यवादी धर्म को नहीं मानते है।
- साम्यवादियों के अनुसार धर्म अफीम है।
- साम्यवाद वर्ग संघर्ष को मानता है।
- साम्यवाद में संसाधनों का समान या आवश्यकता के अनुसार वितरण किया गया है।
- साम्यवाद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है।
- साम्यवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास करता है।
(II) समाजवाद (Socialism)-
- समाजवाद हिंसा का विरोध करता है।
- समाजवाद लोकतांत्रिक आन्दोलन का समर्थन करता है।
- समाजवाद उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को मान्यता देता है।
- समाजवाद राष्ट्रवाद को मानता है।
- समाजवादी धर्म का समर्थन करते है।
- समाजवादी वर्ग संघर्ष तथा वर्ग सहयोग दोनों को मानते है।
- समाजवाद में संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण किया जाता है।
- समाजवाद कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण प्रदान करता है।
- समाजवाद लोकतंत्र को समर्थन करता है।
माओवाद (Maoism)-
- माओवाद समाजवाद का ही एक रूप है।
- माओवाद का प्रवर्तक माओ जेदोंगे तुंग या माओ से-तुंग या माओ जेडोंग था।
- 1 अक्टूबर, 1949 को माओ जेदोंगे के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई थी।
माओवाद निम्नलिखित मामलों में मार्क्सवाद से अलग है।-
- माओवाद के अनुसार किसान भी क्रांति कर सकते है। जबकि मार्क्स के अनुसार औद्योगीकरण का चरम विकास होने पर मजदूर क्रांति कर सकते है।
- माओवाद राष्ट्रवाद में विश्वास करता है।
- माओवाद विश्व क्रांति का समर्थन नहीं करता है।
- माओवाद के अनुसार एक ही देश में साम्यवाद सुरक्षित रह सकता है।
- भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है।
- भारत में विधि का शासन है।
- भारत में विधि के समक्ष सभी समान है।
- भारत में धर्म के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है।
- लोकनियोजन में सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते है।
- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है।
- राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगाता है।
- भारत में सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किन्तु भारतीय पंथनिरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है क्योंकि दोनों जगह अलग-अलग कारणों से पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया है।
- पश्चिमी जगत ने पुनर्जागरण, धर्म सुधार आन्दोलन, प्रबोधन के कारण पंथनिरपेक्षता को अपनाया।
- पंथनिरपेक्षता में यह माना गया की धर्म आस्था का विषय है इसमें तार्किकता को अधिक महत्व नहीं दिया गया इसलिए अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई अतः धर्म को राज्य से पृथक किया गया तथा इसे व्यक्तिगत विषय माना गया और राज्य विधि निर्माण के समय धार्मिक मान्यताओं को महत्व नहीं देगा बल्कि विधि निर्माण का आधार मानववाद व वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए।
- भारत में सभी धर्मों के लोग रहते है अतः धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त हो इसलिए पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया है।
- भारत में धर्म को राज्य से पृथक नहीं किया गया है बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। अतः भारत की पंथनिरपेक्षता 'सर्वधर्म समभाव' है। यही कारण है की राज्य धार्मिक पहचान को मान्यता देता है तथा अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है।
- भारत में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग नागरिक संहिताएँ है।
- राज्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है।
- धर्म शब्द की उत्पति 'धृ' धातु से हुई है जिसका अर्थ है, धारण करने योग अर्थात् कर्त्तव्य। इसलिए Secularism का हिन्दी अनुवाद पंथनिरपेक्षता है न की धर्म निरपेक्षता है।
4. लोकतंत्र (Democracy)-
- जनता का , जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है।
- लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। जैसे-
- (I) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)
- (II) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)
- यदि शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् कार्यपालिका तथा विधायिका से संबधित महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा लिये जाते है प्रतय्क्ष लोकतंत्र कहलाता है।
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में सम्भव हो सकता है लेकिन भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत है। तथा भारत में जनसंख्या भी अधिक है, भारत में संचार के साधनों की कमी भी है साथ ही भारत में लोगों में शिक्षा व राजनीतिक विषयों की समझ भी कम है अतः भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नहीं है।
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्नलिखित रूप है।
- (A) रेफरेंडम या परिपृच्छा (Referendum)
- (B) प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह (Plebiscite)
- (C) राइट टू रिकॉल (Right to Recall)
- (D) इनिशिएटिव या पहल (Initiative)
- जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी हो रेफरेंडम कहलाता है।
- रेफरेंडम का प्रयोग प्रायः विदेशी मामलों में किया जाता है।
- रेफरेंडम को ही परिपृच्छा कहा जाता है।
- जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी न हो प्लेबिसाइट कहलाता है।
- प्लेबिसाइट को ही जनमत संग्रह कहा जाता है।
- प्लेबिसाइट का प्रयोग घरेलू नीति निर्माण से संबंधित मामलों में किया जाता है।
(C) राइट टू रिकॉल (Right to Recall)-
- जनता के पास यह अधिकार होता है की वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व वापस बुला सकती है जिसे राइट टू रिकॉल कहा जाता है। अर्थात् राइट टू रिकॉल के माध्यम से जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटा सकती है।
- भारत में हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में 2020 में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू की गई थी।
(D) इनिशिएटिव या पहल (Initiative)-
- इनिशिएटिव में विधि निर्माण करने के लिए जनता को पहल करने का अधिकार दिया जाता है।
- यदि निश्चित संख्या में जनता किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देती है तो उस प्रस्ताव को विधायिका में पेश किया जाना बाध्यकारी होता है।
- इनिशिएटिव का प्रावधान स्विट्जरलैंड में है।
(II) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)-
- यदि शासन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यदि कार्यपालिका व विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते है तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते है।
- भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अर्द्ध-परिसंघीय ढाँचा अपनाया गया है।
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक रूप होते है जैसे-
- (A) संसदीय शासन व्यवस्था- भारत, ब्रिटेन
- (B) अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था- अमेरिका
- (C) दोहरी कार्यपालिका- फ्रांस
- (D) बहुल कार्यपालिका- स्विट्जरलैंड
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक अन्य रूप में भी बाँटा जा सकता है। जैसे-
- (A) एकात्मक शासन व्यवस्था (Unitary Governance)
- (B) परिसंघीय शासन व्यवस्था (Federal Governance)
(A) एकात्मक शासन व्यवस्था (Unitary Governance)-
- एकात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां केन्द्र सरकार में निहित होती है। जैसे- ब्रिटेन
(B) परिसंघीय शासन व्यवस्था (Federal Governance)-
- परिसंघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे- अमेरिका
5. गणराज्य (Republic)-
- यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है तो उस देश को गणतंत्र कहा जाता है।
- गणराज्य को राजतंत्र की विरोधी विचारधारा माना जाता है क्योंकि गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है और लोकतंत्र में जनता की शासन में भागीदारी होती है।
- ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है।
- चीन में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि चीन के शासन में जनता की भागीदारी नहीं है। लेकिन चीन गणतंत्र है क्योंकि चीन में वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं है।
- लोकतांत्रिक राज्य जैसे- भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि।
- राजतंत्र राज्य जैसे- ब्रुनेई
6. न्याय (Justice)-
- प्रस्तावना में न्याय के निम्नलिखित प्रकार दिए गए है। जैसे-
- (I) सामाजिक न्याय (Social Justice)
- (II) आर्थिक न्याय (Economic Justice)
- (III) राजनीतिक न्याय (Political Justice)
(I) सामाजिक न्याय (Social Justice)-
- एक ऐसा समाज जिसमें निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाता हो-
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, रंग, आयु, लैंगिक रूझान (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल) आदि।
- समाज में समानता हो तथा समाज सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं, अंधविश्वासो, आडम्बरों आदि से मुक्त हो।
- व्यक्ति को विकास हेतु स्वच्छ व स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो।
(II) आर्थिक न्याय (Economic Justice)-
- आर्थिक न्याय से तात्पर्य है की संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात् योग्यता के आधार पर वितरण लेकिन साथ ही वंचित व कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाए।
- आर्थिक न्याय में सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, आर्थिक शोषण का अभाव हो न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित हो, सभी की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो, धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण न हो।
(III) राजनीतिक न्याय (Political Justice)-
- राजनीतिक न्याय के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को मतदान करने व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली हो, चुनावों में धनबल व बाहुबल का प्रयोग न हो, चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद व साम्प्रदायिकता आदि का प्रयोग न हो।
- राजनीतिक न्याय के अंतर्गत देश में चुनाव विकास के मुद्दों पर सम्पन्न हो।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचनाएं (Criticism of Preamble of Indian Constitution)-
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक नहीं है बल्कि प्रस्तावना नकल है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है तथा प्रस्तावना का शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
- प्रस्तावना संविधान का भाग होते हुए भी अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है क्योंकि प्रस्तावना न ही संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्तियों पर कोई अंकुश लगाती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात् भारत के संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारत एक साम्यवादी देश नहीं है। भारत निजी सम्पत्ति को मान्यता देता है और भारत में आर्थिक असमानता है तथा वर्ष 1991 के बाद भारत लगातार पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। अतः समाजवाद शब्द अप्रासंगिक हो गया है।
- 'पंथनिरपेक्षता' शब्द का भी अर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारत में धर्म को राज्य से पृथक नहीं किया गया है बल्कि राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देता है तथा नागरिक संहिताएं धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। अतः विधि के समक्ष समता भी नहीं है
जन्मकुंडली-
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के. एम. मुंशी ने जन्मकुंडली कहा है।
संविधान एक पवित्र दस्तावेज-
- महात्मा गाँधी ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है।
संविधान की आत्मा-
- संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।
42वां संविधान संशोधन-
- भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन सन् 1976 में किया गया था।
- भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके तीन नए शब्द जोड़े गए थे जैसे-
- (I) समाजवादी (Socialist)
- (II) पंथनिरपेक्ष (Secular)
- (III) अखण्डता (Integrity)
- भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान (Mini Constitution) भी कहा जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में अत्यधित परिवर्तन किए गये थे।
- बेरुवाड़ी वाद (Berubari Case) 1960 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है।
- केशवानंद भारती केस (Kesavananda Bharati Case) 1973 उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदलते हुए माना की प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। किन्तु प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है।
- प्रस्तावना न तो संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्ति पर कोई अंकुश लगाती है।
- न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। (प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है/ गैर न्यायोचित/ वाद योग्य नहीं है)
प्रस्तावना में संशोधन-
- केशवानंद भारती वाद या केशवानंद भारती केस 1973 के बाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन किसी भी परिवर्तन से भारतीय संविधान के मूल ढाँचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात् भारतीय संविधान के मूल ढाँचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-
- प्रस्तावना का स्वतंत्र रूप से कोई विधिक प्रभाव नहीं है क्योंकि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है या परिवर्तनीय नहीं है या गैर न्यायोचित है।
- प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है जो की 42वें संविधान संशोधन 1976 से किया गया था।
- प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई है।
- 1994 के एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ वाद में कहा गया की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा प्रस्तावना में लिखा पंथनिरपेक्षता शब्द संविधान के मूल ढांचे का भाग है।
- एम हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है।
- ठाकुरदास भार्गव ने भी प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है।
- एम हिदायतुल्ला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।
- के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा है।
- सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या आधारशिला कहा है।
- नानी पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
- बार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट (Key Note) कहा है।
- आत्म- एम हिदायतुल्ला व ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है।
- आत्मा व हृदय- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया है।
- आत्मा व दर्शन- राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा व दर्शन कहा गया है।