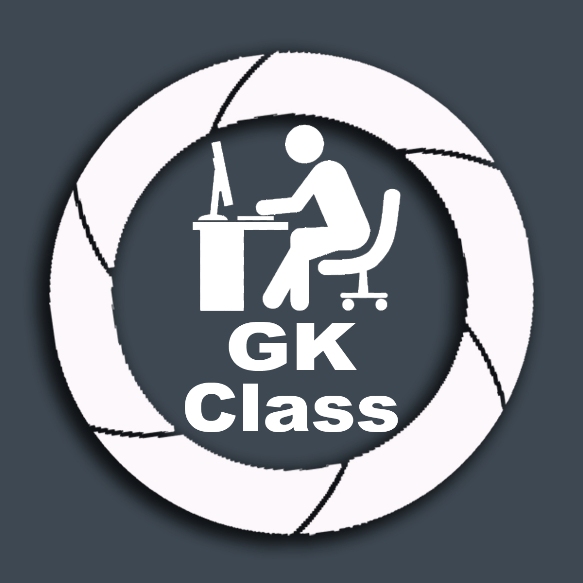मूल अधिकारों में संशोधन या मौलिक अधिकारों में संशोधन (Amendment In Fundamental Rights)-
- मूल अधिकार व मौलिक अधिकार दोनों का अर्थ एक ही है।
- मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग- 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में किया गया है।
अनुच्छेद 13 (2) (Article 13-2)-
- अनुच्छेद 13 (2) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-3 में किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के अनुसार संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो।
अनुच्छेद 368 (Article 368)-
- अनुच्छेद 368 का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग- 20 में किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 (Shankari Prasad Vs Union of India 1995)-
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले या केस का निर्णय सन् 1951 में दिया गया था।
- शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया की अनुच्छेद 13 (2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है संविधान संशोधन अधिनियम पर नहीं। अर्थात् संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीमित कर सकती है।
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 (Sajjan Singh Vs State of Rajasthan 1965)-
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामले या केस का निर्णय सन् 1965 में दिया गया था।
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया अर्थात् संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीमित कर सकती है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 (Golaknath Vs State of Punjab 1967)-
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले या केस का निर्णय सन् 1967 में दिया गया था।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना की संविधान संशोधन अधिनियम भी एक विधि है अतः अनुच्छेद 13 (2) संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होता है। अर्थात् संसद संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार नहीं देता है लेकिन अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संशोधन की शक्ति सामान्य विधायी शक्ति से प्राप्त होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया की गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में दिये दये निर्णन को भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात् गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के निर्णय से पहले मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों में जो कटौती की गई है वह यथावत् रहेगी लेकिन भविष्य में संसद मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है।
24वां संविधान संशोधन 1971 (24th Constitution Amendment 1971)-
- भारतीय संविधान में 24वां संविधान संशोधन सन् 1971 में किया गया था।
- 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 (4) तथा अनुच्छेद 368 (3) भारतीय संविधान में जोड़े गये थे।
- 24वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था की अनुच्छेद 13 (2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। और अनुच्छेद 368 के तहत किए गये संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है।
- 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया की राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है।
25वां संविधान संशोधन 1971 (25th Constitution Amendment 1971)-
- भारतीय संविधान में 25वां संविधान संशोधन सन् 1971 में किया गया था।
- 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 (C) जोड़ा गया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 (C) में यह प्रावधान किया गया की अनुच्छेद 39 (b) व अनुच्छेद 39 (c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है और इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर अधिनियम असंवैधानिक नहीं है।
- इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 (Kesavananda Bharti Vs State of Kerala 1973)-
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले या केस का निर्णय सन् 1973 में दिया गया था।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय में 24वें संविधान संशोधन तथा 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के लिए सर्वोच्च न्यायालय में 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में गठित की गई 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन तथा 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक ठहराया अर्थात् यह माना की अनुच्छेद 368 के तहत किए गये संविधान संशोधन के द्वारा संसद मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। लेकिन न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है।
- 25वें संविधान संशोधन 1971 के दूसरे भाग को न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा या मूल ढांचा है।
42वां संविधान संशोधन 1976 (42th Constitution Amendment 1976)-
- भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन सन् 1976 में किया गया था।
- 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 (C) का विस्तार किया गया था।
- 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 (C) में यह प्रावधान किया गया था की सभी नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है तथा संसद के द्वारा बनाई गई विधि से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नही होगा
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 (Minerva Mills Vs Union of India 1980)-
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले या केस में निर्णय सन् 1980 में दिया गया था।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 31 (C) में किये गए विस्तार को चुनौती दी गई थी।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 (C) में किये गए विस्तार को अंसवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31 (C) को पूर्ववर्ती रूप में पुनः स्थापित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना की मूल अधिकार या मौलिक अधिकार व राज्य की नीति के निदेशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है। मूल अधिकार व राज्य की नीति के निदेशक तत्व दोनों के उद्देश्य (मानव कल्याण) समान है। अतः मूल अधिकार व राज्य की नीति के निदेशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है।
- यदि मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों व राज्य की नीति के निदेशक तत्व दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Link)-