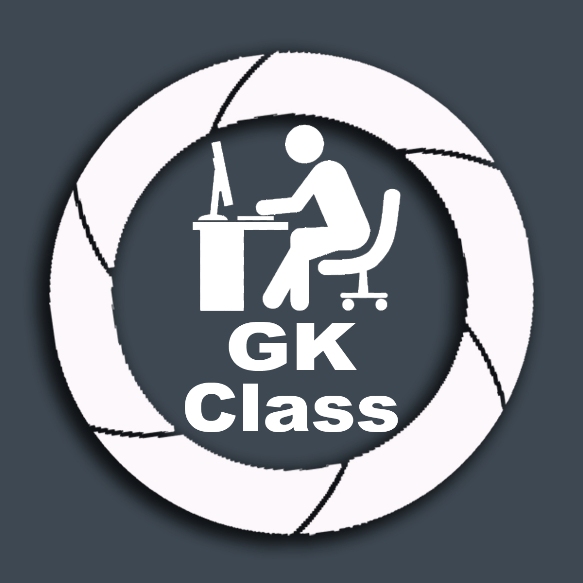उच्च न्यायालय (High Court)-
- भारत के संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग-6 तथा अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है।
- वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 25 उच्च न्यायालय है।
- सन् 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। जैसे-
- (I) कलकता (Calcutta)
- (II) बॉम्बे (Bombay)
- (III) मद्रास (Madras)
- सन् 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- सन् 1947 से पहले भारत में 11 प्रान्त थे सभी प्रान्तों में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। अर्थात् सन् 1947 में 11 प्रान्त में 11 उच्च न्यायालय थे।
- वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है।
- वर्ष 2019 में 25वां उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बनाया गया है।
- वर्ष 2013 में भारत में तीन उच्च न्यायालय बनाये गये थे। जैसे-
- (I) त्रिपुरा (Tripura)
- (II) मणिपुर (Manipur)
- (III) मेघालय (Meghalaya)
अनुच्छेद 214-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
7वां संविधान संशोधन 1956-
- 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है।
राज्य (States) तथा संघ क्षेत्र (UTs) के प्रमुख उच्च न्यायालय-
- 1. गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court)
- 2. बोम्बे उच्च न्यायालय (Bombay Hight Court)
- 3. कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court)
- 4. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court)
- 5. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)
- 6. केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court)
- 7. जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय (Jammu & Kashmir and Ladakh High Court)
1. गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court)-
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) असम (Assam)
- (II) अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)
- (III) नागालैण्ड (Nagaland)
- (VI) मिजोरम (Mizoram)
2. बोम्बे उच्च न्यायालय (Bombay Hight Court)-
- बोम्बे उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) महाराष्ट्र (Maharashtra)
- (II) गोवा (Goa)
- (III) दमन दीव (Daman-Diu) और दादरा नगर हवेली (Dadar Nagar Haveli)
3. कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court)-
- कलकत्ता उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) पश्चिम बंगाल (West Bengal)
- (II) अण्डमान एवं निकोबार (Andaman and Nicobar)
4. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court)-
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) पंजाब (Punjab)
- (II) हरियाणा (Haryana)
- (III) चंडीगढ (Chandigarh)
5. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)-
- मद्रास उच्च न्यायालय में निम्नलिकित राज्य या UT शामिल है।
- (I) तमिलनाडु (Tamil Nadu)
- (II) पुदुचेरी (Puducherry)
6. केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court)-
- केरल उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) केरल (Kerala)
- (II) लक्षद्वीप (Lakshadweep)
7. जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय (Jammu & Kashmir and Ladakh High Court)-
- जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राज्य या UT शामिल है।
- (I) जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir)
- (II) लद्दाख (Ladakh)
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Hight Court Judges)-
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) + 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- स्थानांतरण (Transfer)- कॉलेजियम के द्वारा (दोनों HC के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
न्यायाधीश का कार्यकाल (Tenure of Judge) (Tenure)-
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
- 62 वर्ष की आयु सीमा तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं।
न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (Process of Removal of Judge)-
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं (Qualifications of a High Court Judge)-
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। या न्यूनतम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो।
उच्च न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction of High Court)-
- उच्च न्ययाालय की अधिकारिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 में किया गया है।
- (अ) आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction)
- (ब) अपीलिय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction)
(अ) आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction)-
- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, कम्पनी मामले
- नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
- सांसदों व राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
- राजस्व विषय तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले।
- अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भेजे गए मामले।
- निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को एक राशि के दीवानी मामलों में आरम्भिक अधिकारिता है।-
- (I) दिल्ली (Delhi)
- (II) मद्रास (Madras)
- (III) कलकत्ता (Calcutta)
- (IV) बोम्बे (Bombay)
- सन् 1973 से पहले निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक मामलों में भी आरम्भिक अधिकारिता थी।-
- (I) मद्रास (Madras)
- (II) बोम्बे (Bombay)
- (III) कलकत्ता (Calcutta)
- सन् 1973 में इसे समाप्त कर दिया गया। (उपर्युक्त तीनों में आपराधिक मामलों में भी आरम्भिक अधिकारिता समाप्त कर दी गई)
(ब) अपीलिय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction)-
- जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है।
- निम्नलिखित 2 प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है।-
- (I) दीवानी मामले (Civil Matters)- इसमें प्रथम व द्वितीय अपीत दोनों प्रकार की अपील हो सकती है।
- (अ) प्रथम अपील (First Appeals)- जिसमें तथ्यों का प्रश्न (Question of Fact) व विधि का प्रश्न (Question of Law) दोनों निहित होते हैं।
- (ब) द्वितीय अपील (Second Appeals)- इसमें केवल विधि का प्रश्न निहित होता है।
- दीवानी मामलों में निम्नलिखित तीन उच्च न्यायालयों में एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध खण्डपीठ में अपील की जा सकती है।
- (अ) कलकत्ता (Calcutta)
- (ब) बोम्बे (Bombay)
- (स) मद्रास (Madras)
- सन् 1997 में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक एवं दूसरे अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है।
- (II) आपराधिक मामले (Criminal Matters)- जिन मुकदमों में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, उनके लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- मृत्युदण्ड के सभी मामलों में उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है।
रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction)-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जैसे-
- (I) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (II) परमादेश (Mandamus)
- (III) प्रतिषेध (Prohibition)
- (IV) उत्प्रेषण (Certiorari)
- (V) अधिकारपृच्छा (Quo-warranto)
- चन्द्रकुमार वाद 1997 (Chandrakumar Case 1997)- रिट अधिकारिता संविधान का मूल ढाँचा है।
अनुच्छेद 215-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 में अभिलेखिय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना (High Courts to be a Court of Record) का उल्लेख किया गया है।
- उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे।
- अन्य न्यायालय उन निर्णयों की समीक्षा या आलोचना नहीं कर सकते हैं।
- न्यायालय की अवमानना पर 6 माह की सजा अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।
न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)- अनुच्छेद [226, 13 (2)]
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 व 13 (2) में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है।
- उच्च न्यायालय संसद व राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है तथा संविधान के विरोधी होने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकता है।
- यह निर्णय केवल राज्य में लागू होंगे।
- उच्च न्यायालय राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है।
42वां संशोधन- 1976
- 42वें संविधान संशोधन 1976 में केंद्रीय कानूनों के पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दिया गया था।
43वां संशोधन- 1977
- 43वें संविधान संशोधन 1977 में केंद्रीय कानूनों के पुनरावलोकन की शक्ति वापस प्रदान कर दी गई थी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-
- स्वतंत्रता के बाद पहला नया उच्च न्यायालय ओडिशा उच्च न्यायालय बना था। (1948)
- स्वतंत्रता के बाद दूसरा नया उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय बना था। (1949)
- भारत में कुल 3 उच्च न्यायालय ऐसे है जो एक से अधिक राज्य के लिए कार्य करते हैं। जैसे-
- (I) गुवाहाटी उच्च न्यायालय- असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम
- (II) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (चंडीगढ़)- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
- (III) बॉम्बे उच्च न्यायालय- महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
- अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय कार्य करता है।
- लक्षद्वीप के लिए केरल उच्च न्यायालय कार्य करता है।
- पुडुचेरी के लिए मद्रास मद्रास उच्च न्यायालय कार्य करता है।
- भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय है।
- भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है।
- भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख रुपये है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपये है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है।